दशरथनंदन श्रीराम
परमात्मा की लीला को कौन समझ सकता है। हमारे जीवन की सभी घटनाएं प्रभु की लीला का ही एक लघु अंश है। महर्षि वाल्मीकि की राम को सरल बोलचाल की भाषा में लोगों तक पहुंचाने की मेरी इच्छा हुई। विद्वान् न होने पर भी वैसा करने की धृष्टता कर रहा हूं। कबन ने अपने काव्य के प्रारंभ में विनय की जो बात कही है, उसीको में अपने लिए भी यहां दोहराना चाहता हूँ। वाल्मीकि रामायण को तमिल भाषा में लिखने का मेरा लालच वैसा ही है, जैसे कोई बिल्ली विशाल सागर को अपनी जीभ से चाट जाने की तृष्णा करे । फिर भी मुझे विश्वास है कि जो श्रद्धा-भक्ति के साथ रामायण कथा पढ़ना चाहते हैं, उन सबकी सहायता, अनायास ही, समुद्र लांघनेवाले मारुति करेंगे। बड़ों से मेरी विनती है कि वे मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और मुझे प्रोत्साहित करें, तभी मेरी सेवा लाभप्रद हो सकती है। समस्त जीव-जंतु तथा पेड़-पौधे दो प्रकार के होते हैं। कुछ के हड्डिया बाहर होती हैं और मांस भीतर । केला, नारियल, ईख आदि इसी श्रेणी में आते हैं। कुछ पानी के जंतु भी इसी वर्ग के होते हैं। इनके विपरीत कुछ पौधों और हमारे जैसे प्राणियों का मांस बाहर रहता है और हड़ियां अंदर इस प्रकार आवश्यक प्राण तत्त्वों को हम कहीं बाहर पाते हैं, कहीं अंदर इसी प्रकार ग्रंथों को भी हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। कुछ ग्रंथों का प्राण उनके भीतर अर्थात् भावों में होता है, कुछ का जीवन उनके बाह्य रूप में रसायन, वैद्यक, गणित, इतिहास, भूगोल आदि भौतिक शास्त्र के ग्रंथ प्रथम श्रेणी के होते हैं। भाव का महत्व रखते हैं। उनके रुपांतर से विशेष हानि नहीं हो सकती, परंतु काव्यों की बात दूसरी होती है। उनका प्राण अथवा महत्त्व उनके रूप पर निर्भर रहता है। इसलिए पद्य का गद्य में विश्लेषण करना खतरनाक है। फिर भी कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, जो दोनों कोटियों में रहकर लाभ पहुंचाते हैं। जैसे तामिल में एक कहावत है–‘हाथी मृत हो या जीवित दोनों अवस्थाओं में अपना मूल्य नहीं खोता ।’ वाल्मीकि रामायण भी इसी प्रकार का ग्रंथ रत्न है; उसे दूसरी भाषाओं में गद्य में कहें या पद्य में, वह अपना मूल्य नहीं खोता। पौराणिक का मत है कि वाल्मीकि ने रामायण उन्हीं दिनों लिखी, जबकि श्रीरामचन्द्र पृथ्वी पर अवतरित होकर मानव-जीवन व्यतीत कर रहे थे, किन्तु सांसारिक अनुभवों के आधार पर सोचने से ऐसा लगता है कि सीता और राम की कहानी महर्षि वाल्मीकि के बहुत समय पूर्व से भी लोगों में प्रचलित थी, लिखी भले ही न गई हो। ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों में परंपरा से प्रचलित कथा को कवि वाल्मीकि के काव्यबद्ध किया । कारण रामायण-कथा में कुछ उलझने जैसे बालि का वध तथा सीताजी को वन में छोड़ आना जैसी न्यायविरुद्ध बातें घुस गई हैं।
महर्षि वाल्मीकि ने अपने काव्य में राम को ईश्वर का अवतार नहीं माना। हा स्थान-स्थान पर वाल्मीकि की रामायण में हम रामचन्द्र को एक यशस्वी राजकुमार, अलौकिक और असाधारण गुणों से विभूषित मनुष्य के रूप में ही देखते हैं। ईश्वर के स्थान में अपने को मानकर राम ने कोई काम नहीं किया वाल्मीकि के समय में ही लोग राम को भगवान मानने लग गये थे। वाल्मीकि के इन दो ग्रंथ सैकड़ों वर्ष पश्चात् हिन्दी में संत तुलसीदास ने और तमिल के कंबन ने राम चरित जिनमें मैंने गाया । तबतक तो लोगों के दिलो में यह पक्की धारणा बन गई थी कि राम भगवान नारायण के अवतार थे। लोगों ने राम में और कृष्ण में या भगवान विष्णु में भिन्नता हुई है। जो देखना ही छोड़ दिया था भक्ति मार्ग का उदय हुआ। मंदिर और पूजा-पद्धति भी स्थापित हुई।ऐसे समय में तुलसीदास अथवा कंचन रामचंद्र को केवल एक वीर मानव समझकर काव्य-रचना कैसे करते ? दोनों केवल कवि ही नहीं थे, वे पूर्णतया भगवद्भक्त भी थे। वे आजकल के उपन्यासकार अथवा अन्वेषक नहीं थे। श्रीराम को केवल मनुष्यत्व की सीमा में बाप लेना भक्त तुलसीदास अथवा कंबन के लिए अशक्य बात थी। इसी कारण अवतार-महिमा को इन दोनों के सुंदर रूप में गद्गद कंठ से कई स्थानों पर गाया है।
महर्षि वाल्मीकि की रामायण और कंबन-रचित रामायण में जो भिन्नताएं हैं, वे इस प्रकार हैं; वाल्मीकि रामायण के छंद समान गति से चलनेवाले हैं, कंबन के काव्य-छंदों को हम नृत्य के लिए उपयुक्त कह सकते हैं, वाल्मीकि की शैली में गांभीर्य है, उसे अतुकांत लोगों को कह सकते हैं. बंबन की शैली में जगह-जगह नूतनता है, वह ध्वनि-माधुरी-संपन्न है, आभूषण से अलंकृत नर्तकी के नृत्य के समान वह मन को लुभा लेती है, साथ-साथ भक्तिमान की प्रेरणा भी देती जाती है, किंतु कंचन की रामायण तमिल लोगों की ही समझ में आ सकती है। कंबन की रचना को इतर भाषा में अनूदित करना अथवा तमिल में ही गय-रूप में परिणत करना लाभप्रद नहीं हो सकता। कविताओं को सरल भाषा समझाकर फिर मूल कविताओं को गाकर बतायें, तो विशेष लाभ हो सकता है। किन्तु यह काम तो केवल श्री टी० के० चिदंबरनाथ मुदलियार ही कर सकते थे। अब तो वह रहे नहीं। सियाराम, हनुमान और भरत को छोड़कर हमारी और कोई गति नहीं। हमारे मन की शांति, हमारा सबकुछ उन्हीं के ध्यान में निहित है। उनकी पुण्य कथा हमारे पूर्वजों की परोहर है। इसी के आधार पर हम आज जीवित हैं। जबतक हमारी भारत भूमि में गंगा और कावेरी प्रवहमान हैं, तबतक सीता-राम की कथा भी आबात, स्त्री-पुरुष, सबमें प्रचलित रहेगी, माता की तरह हमारी जनता की रक्षा करती रहेगी। मित्रों की मान्यता है कि मैंने देश की अनेक सेवाएं की है, लेकिन मेरा मत है कि भारतीय इतिहास के महान एवं घटनापूर्ण काल में अपने व्यस्त जीवन की सांध्यवेला में इन दो ग्रंथों (‘व्यासर्विरूंदु’ महाभारत और ‘चक्रवर्ति तिरुमगन्-रामायण) की रचना, जिनमें मैंने महाभारत तथा रामायण की कहानी कही है, मेरी राय में, भारतवासियों के प्रति की गई मेरी सर्वोत्तम सेवा है और इसी कार्य में मुझे मन की शांति और तृप्ति प्राप्त हुई है। जो हो, मुझे जिस परम आनंद की अनुभूति हुई है, वह इनमें मूर्त्तिमान है, कारण कि इन दो ग्रंथों में मैंने अपने महान संतों द्वारा हमारे प्रियजनों, स्त्रियों और पुरुषों से, अपनी ही भाषा में एक बार फिर बात करनेकुंती, कौसल्या, द्रौपदी और सीता पर पड़ी विपदाओं के द्वारा लोगों के मस्तिष्कों को परिष्कृत करने में सहायता की है। वर्तमान समय की वास्तविक आवश्यकता यह है कि हमारे और हमारी भूमि के संतों के बीच ऐक्य स्थापित हो, जिससे हमारे भविष्य का निर्माण मजबूत चहान पर हो सके, बालू पर नहीं । हम सीता माता का ध्यान करें। दोष हम सभी में विद्यमान है। मां सीता की शरण के अतिरिक्त हमारी दूसरी कोई गति ही नहीं उन्होंने स्वयं कहा है, भूते किससे नहीं होती ? दयामय देवी हमारी अवश्य रक्षा करेंगी। दोषों और कमियों से भरपूर अपनी इस पुस्तक को देवी के चरणों में समर्पित करके मैं नमस्कार करता हूं। मेरी सेवा में लोगो को लाभ मिले
-चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य















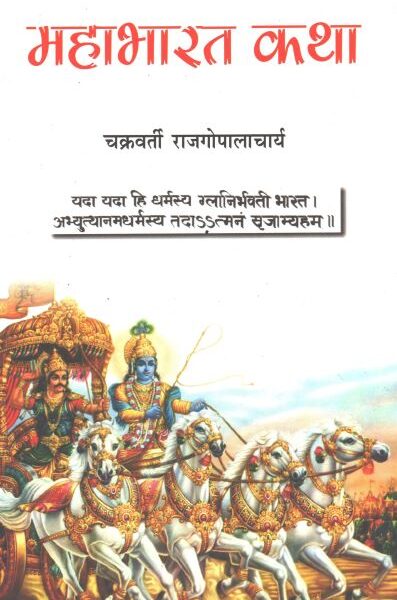
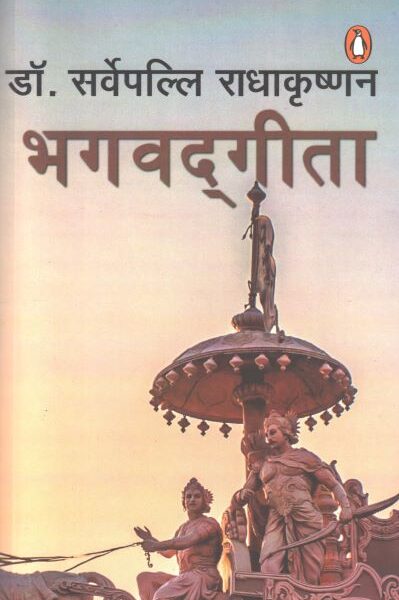


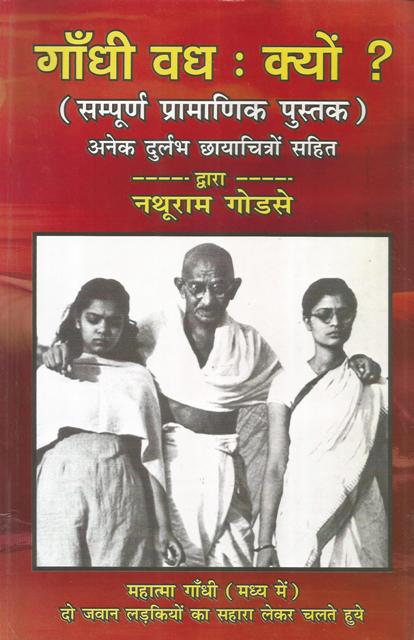
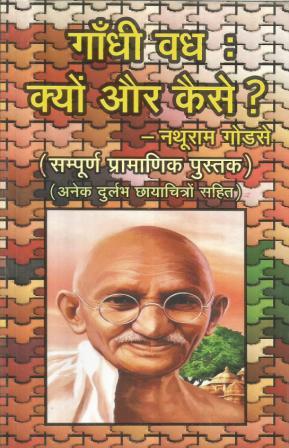
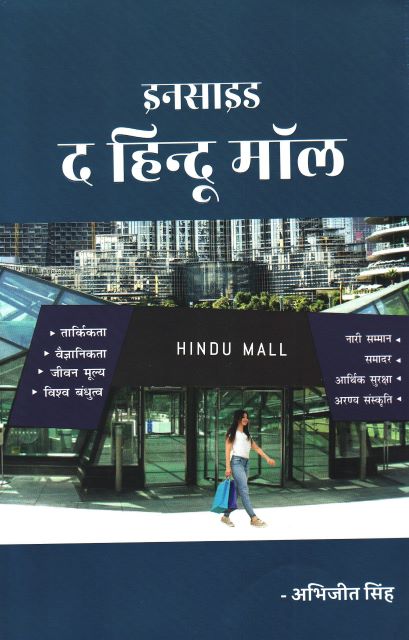

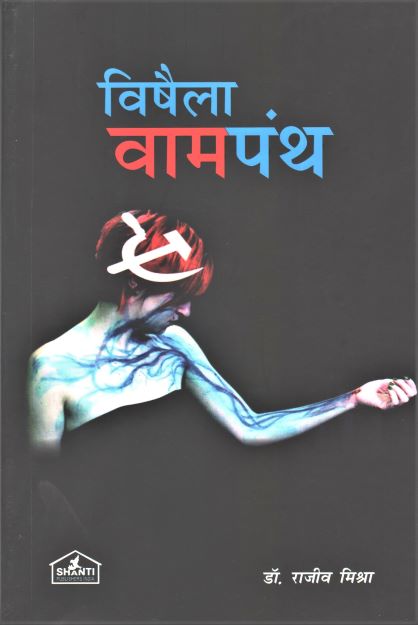
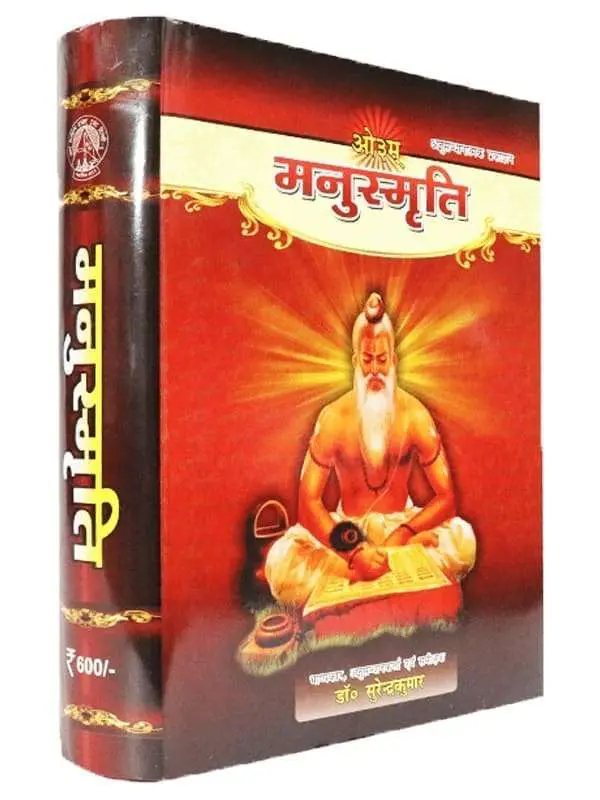
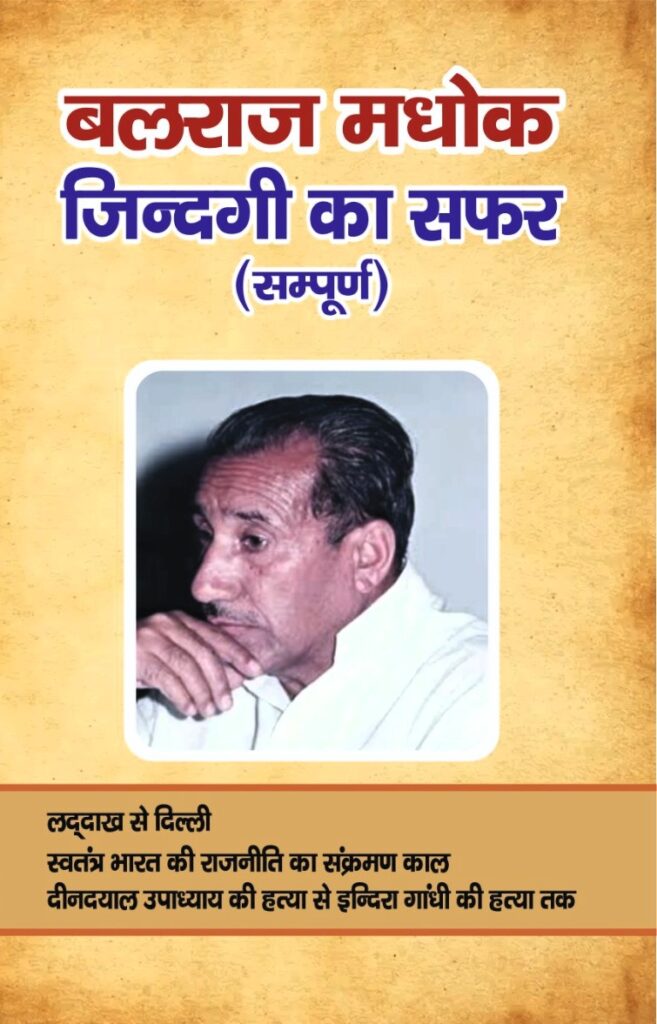
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.